मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व में अंतर | Difference Between Fundamental Rights and Directive Principles :- किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक विधान होना चाहिए। जिसका सही से उपयोग हो।
जिसमें उस राज्य के सभी मूल अधिकार एवं सब कर्तव्य का अक्षर से वर्णन किया गया हो नागरिकों को हर संभव मदद एवं उनके उत्थान के लिए कार्य किया गया हो। इन्हीं सब को बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर (Difference Between Fundamental Rights and Directive Principles) लेकर आए हुए हैं। आशा करता हूं कि यह टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो।
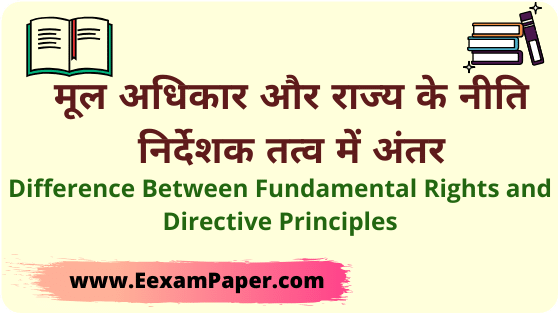
मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व में अंतर | Difference Between Fundamental Rights and Directive Principles
हम आपको इस बात से अवगत करा दें कि अगर आपको मौलिक अधिकार एवं राज्य में निर्देशक तत्व के बीच का अंतर (Difference Between Fundamental Rights and Directive Principles) जानना है तो आपको इस बात को सर्वप्रथम समझना होगा कि, मूल अधिकार किसे कहते हैं? तथा यह संविधान में कितने रूपों में वर्णित है। इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में भी आप को समझना होगा और इनसे संबंधित अनुच्छेदों को पढ़ना और जानना होगा।
मूल अधिकार :-
संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इस संबंध में भारतीय संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान में वर्णित अधिकार पत्र, 1791 ई० (Bill of Rights) से प्रभावित है। मूल अधिकारों (Fundamental Rights) का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। यह अधिकार देश में लोग व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है।
संविधान के भाग – 3 को भारत का मैग्नाकार्टा (Magnacarta of India) कहा जाता है। मूल अधिकार भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है किंतु इसे संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है।
- अनुच्छेद 12 – राज्य की परिभाषा
- अनुच्छेद – 13 ( मूलाधिकारों से असंगत तथा अल्पीकरण करने वाली विधियां)
- अनुच्छेद – 14 – 18 ( समानता का अधिकार )
- अनुच्छेद – 19 – 22 ( स्वतंत्रता का अधिकार )
- अनुच्छेद – 23 – 24 ( शोषण के विरुद्ध )
- अनुच्छेद – 25 – 28 ( धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार )
- अनुच्छेद – 29 – 30 ( संस्कृति और शिक्षा संबंधी ) अधिकार )
- अनुच्छेद – 32 ( संवैधानिक उपचारों का अधिकार )
डॉ भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व :-
भारतीय संविधान राज्य की शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए नीति निर्देशक तत्व (Directive Principales of State Policy) का प्रावधान किया गया है। राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य – सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। यह उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है जैसा कि संविधान निर्माता भारत को भविष्य में देखना चाहते थे।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग – 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक वर्णित किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व शीर्षक से यह स्पष्ट हो जाता है कि नीति एवं कानून को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखकर बनाएगा।
Difference Between Fundamental Rights and Directive Principles | मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व में अंतर
| मूल अधिकार (Fundamental Rights) | नीति निर्देशक तत्व (Directive Principales of State Policy) |
| यह अपने मूल प्रकृति में नकारात्मक है, क्योंकि यह राज्य को कुछ मामलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं। | यह अपनी मूल प्रकृति में सकारात्मक हैं, क्योंकि राज्य को कुछ मामलों पर इनकी आवश्यकता होती है। |
| यह न्यायोचित होते हैं, इनके हहन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू करवाया जा सकता है। | यह गैर – न्यायोचित होते हैं इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। |
| इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। | इनका उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। |
| यह व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, इस प्रकार यह स्वतः वैयक्तिक होते हैं | यह समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, इस प्रकार यह समाजवादी होते हैं |
| यह कानूनी रूप से मान्य है | इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है |
| इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती है। यह स्वतः लागू हो जाते हैं | इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है यह स्वतः लागू नहीं हो सकते हैं। |
| न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है, कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को गैर संवैधानिक एवं अवैध घोषित करें। | निदेशक तत्वों का उल्लंघन करने वाली किसी विधि को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता। यद्यपि विधि की वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि इन्हें निदेशक तत्व को प्रभावी करने के लागू किया गया था। |
Difference Between Fundamental Rights and Directive Principles से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर
- यौगिक और मिश्रण में अंतर | Difference Between Mixture and Compound
- अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर | Difference between Transverse Wave and longitudinal Wave
- अम्ल और क्षार में अंतर | Difference Between Acid and Base
- हार्मोन और एंजाइम में अंतर | Difference between Hormones and Enzyme
- सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर | Difference Between Scalar and Vector Quantity
- रुधिर और लसीका में अंतर
- उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर | Difference Between Convex And Concave Lens
- डीएनए और आरएनए में अंतर | Difference between D.N.A and R.N.A
- जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर | तुलना | समानता
- धमनी और शिरा में अंतर | Difference Between Arterie And Vein
- गैस और वाष्प में अंतर | वाष्प भाप और गैस में अंतर | Difference Among Gas, Vapour and Steam
- मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व में अंतर | Difference Between Fundamental Rights and Directive Principles
- चाल और वेग में अंतर | Difference Between Speed and Velocity